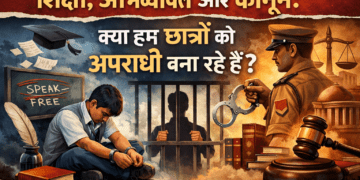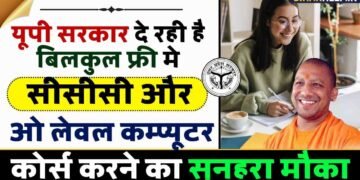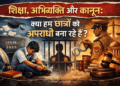भले ही दुनिआ में महिलाये पुरुषो के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कन्धा मिलाकर चल रही है भले ही वो सेना, प्रशासन, पुलिस, खेल या फिर अपराध का ही क्षेत्र क्यों न हो, देश में महिला थाने और महिला जेल इसबात की गवाह है की अपराध करने में महिलाये भी पुरुषो से पीछे नहीं है, सास ससुर, माँ बाप पति भाई की हत्या से लेकर अपने खुद के बच्चो की हत्या तक में महिलाये अग्रणी है, फिर भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। संविधान से लेकर दंड संहिता तक, हर जगह महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान मौजूद हैं। लेकिन कई बार यह सवाल उठता है कि जब कोई महिला अपराधी होती है और पुलिस अपने कर्तव्य का पालन करती है, तब क्या केवल महिला होने के नाते उसके चिल्लाने या आरोप लगाने से पुलिसकर्मी दोषी मान लिया जाए?
हाल ही में दिल्ली से प्रयागराज जा रही ट्रेन में ऐसा मामला सामने आया जिसने इस बहस को और तेज़ कर दिया।
ट्रेन वाला मामला : अनुशासनहीनता या कर्तव्य?
दिल्ली–प्रयागराज ट्रेन में GRP सिपाही आशीष गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने सीट पर सो रही एक युवती को “bad touch” किया। पीड़िता ने तुरंत वीडियो बनाया, जिसमें सिपाही कान पकड़कर माफ़ी माँगता दिखा। घटना सामने आते ही विभाग ने उन्हें निलंबित (Suspended) कर दिया।
इस घटना ने पुलिस बल की छवि पर गहरा असर डाला। क्योंकि यह स्थिति कर्तव्य निर्वहन नहीं बल्कि व्यक्तिगत आचरण की गलती थी। यानी यहाँ पुलिस का बचाव संभव नहीं है।
लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई पुलिसकर्मी महिला अपराधी को पकड़ने के लिए ज़ोर से थामे और वह चिल्लाने लगे, तो समाज और कानून कैसे फैसला करे?
महिला सुरक्षा के विशेष प्रावधान
भारत में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कई सख्त क़ानून बनाए गए हैं, जैसे:
- CrPC की धारा 46 – महिला की गिरफ्तारी के लिए महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति आवश्यक है।
- रात्रि गिरफ्तारी पर रोक – शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले महिला की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, सिवाय मैजिस्ट्रेट की अनुमति के।
- IPC 354, 354A-D, 376 आदि – महिला से छेड़छाड़, बदनीयती से स्पर्श, अश्लील टिप्पणी, पीछा करना और बलात्कार जैसे अपराधों पर सख्त सज़ा।
इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है।
समस्या : कर्तव्य और आरोप में फर्क कैसे किया जाए?
यहीं पर सबसे बड़ी दिक़्क़त आती है।
- Bad Touch बनाम Duty Touch
- अगर पुलिसकर्मी महिला को गलत नियत से छूता है, तो यह अपराध है।
- लेकिन अगर अपराधी महिला को भागने से रोकने या नियंत्रित करने के लिए पुलिस पकड़ती है, तो यह कर्तव्य है।
- समाज अक्सर इन दोनों स्थितियों में फर्क नहीं कर पाता।
- Gender Shield का Misuse
- कई बार महिला अपराधी या संदिग्ध “gender card” खेल लेती है।
- जैसे ही पुलिस पकड़ती है, वह चिल्लाने लगती है – “छेड़छाड़ की है।”
- भीड़ या मीडिया तुरंत महिला की बात को सच मान लेते हैं और पुलिसकर्मी को दोषी ठहरा देते हैं।
- कानून की एकतरफ़ा धारणा
- हमारे समाज और कानून में महिला को भोगी और पुरुष को अपराधी मान लेने की प्रवृत्ति है।
- इससे genuine policing भी शक के घेरे में आ जाती है।
क्यों होती है ऐसी समस्या?
- सामाजिक मानसिकता – लोगों की प्रवृत्ति है कि महिला हमेशा सही होगी और पुरुष पर शक करना चाहिए।
- पुलिस प्रशिक्षण की कमी – कई बार male constable को महिलाओं से जुड़े मामलों को संभालने की संवेदनशील ट्रेनिंग नहीं मिलती।
- मीडिया का दबाव – मीडिया बिना जांच पूरी किए सनसनी फैला देता है। इससे पुलिसकर्मी पहले से ही दबाव में आ जाते हैं।
संभावित समाधान
इस समस्या से बचने के लिए संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।
- महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाना
- अधिक से अधिक महिला constables और officers की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि महिला अपराधियों के मामलों में ambiguity कम हो।
- Body Cameras और CCTV
- अगर हर पुलिसकर्मी के पास body cam हो, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि छूना कर्तव्य था या अशोभनीय हरकत।
- पुलिस प्रशिक्षण में सुधार
- पुलिस को सिखाया जाए कि महिलाओं से जुड़े मामलों को कैसे प्रोफेशनल और संवेदनशील तरीके से हैंडल करना है।
- कानूनी सुधार
- कानून को gender neutral बनाना चाहिए, ताकि पुरुष पुलिसकर्मी भी अपनी innocence साबित कर सके।
- जागरूकता और संतुलन
- समाज को यह समझाना जरूरी है कि हर चिल्लाहट सच नहीं होती और हर पुलिसकर्मी अपराधी नहीं होता।
निष्कर्ष
दिल्ली–प्रयागराज ट्रेन वाला मामला स्पष्ट रूप से सिपाही की गलती था, जिसमें सज़ा मिलना ही चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर बार महिला के आरोप को बिना जांच के सही मान लिया जाए।
महिला सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके नाम पर पुलिस के genuine कर्तव्य को बाधित करना भी गलत है।
हमें एक ऐसा संतुलन बनाना होगा जिसमें –
- महिलाओं की गरिमा सुरक्षित रहे,
- और पुलिस भी बिना डर के अपने कर्तव्यों का पालन कर सके।
👉 असली चुनौती यही है कि कानून और समाज “bad touch” और “duty touch” में फर्क करे। तभी महिला सुरक्षा और न्याय, दोनों का संतुलन बना रहेगा।
हम ये नहीं कहते है की पुरुष अगर अपराध करे तो उसको दंड न दिया जाये, लेकिन झूठे अपराध का आरोप का भी भय इतना नहीं होना चाहिए की व्यक्ति मजबूर हो जाए घुटने टेकने पर, क्युकी लोकतंत्र का मतलब है सभी को न्याय मिले ऐसा न हो की कमजोर समझ कर किसी ढाल दी और वो उसको हथियार बना कर बाकी लोगो पर हमला करने लगे और जब पकड़े जाए तो विक्टिम कार्ड खेलने लगो।