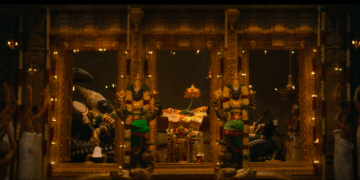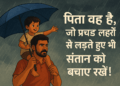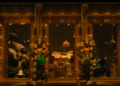आज जब भारत वैश्विक मंच पर अपने गौरवशाली अतीत और सांस्कृतिक धरोहर की पहचान लेकर खड़ा है, तब यह सोचना ज़रूरी हो जाता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, विशेषकर बॉलीवुड, किस दिशा में समाज को प्रेरित कर रही है? आस्था, धर्म और पवित्रता जैसे विषय, जिन पर संतुलन और संवेदनशीलता की अपेक्षा होती है, आज इनका उपयोग सनातन धर्म की छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। यह लेख उसी पक्ष को उजागर करने का एक प्रयास है।
बॉलीवुड में पिछले कुछ वर्षों में ‘ओह माई गॉड’, ‘पीके’, ‘तांडव’, ‘आश्रम’ जैसी कई फिल्में और वेब सीरीज़ बनीं, जिनका मूल स्वर कथित रूप से “कुरीतियों के खिलाफ” था। इन फिल्मों में दिखाया गया कि कैसे धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, कैसे बाबाओं का शोषणकारी रूप समाज में व्याप्त है, और कैसे धर्म व्यापार बन चुका है।
यहाँ तक तो ठीक था – लेकिन चिंताजनक तब होता है जब यह तथाकथित “सुधारवाद” सिर्फ एक ही धर्म, सनातन धर्म के लिए आरक्षित हो जाता है। क्या यही निष्पक्षता है? क्या यही संवैधानिक समता है? जब आस्था का केंद्र सिर्फ सनातन धर्म को बना कर उस पर बार-बार व्यंग्य और हमला किया जाता है, तो यह न सुधार कहलाता है, न कला – बल्कि यह सोची-समझी वैचारिक घेराबंदी बन जाती है।
क्या कुरीतियाँ सिर्फ एक धर्म की हैं?
हर धर्म, हर समाज में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। सुधार की आवश्यकता हर जगह होती है – लेकिन सुधार की आड़ में एक खास आस्था पर एकपक्षीय हमला न तो नैतिक है, न लोकतांत्रिक।
आज हमारे समाज में कई ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो बेहद जघन्य हैं, लेकिन उन्हें कभी उसी तरह से चित्रित नहीं किया जाता जैसे सनातन के मामलों को किया जाता है। उदाहरण के तौर पर:
- अजमेर शरीफ में वर्षों तक नाबालिग हिन्दू लड़कियों के साथ जो हुआ, वह एक समाज की सामूहिक चुप्पी का उदाहरण है।
- सालों पहले CBI ने जागीर कौर केस में सम्मान हत्या का खुलासा किया। एक माँ ने अपनी ही बेटी की हत्या करवाई क्योंकि उसने अंतरजातीय विवाह किया था – क्या उस पर कोई फिल्म बनी?
- बरेली में एक मदरसे के 20 वर्षीय छात्र ने महीनों तक 13 साल के लड़के के साथ यौन शोषण किया – क्या उस पर कोई वेब सीरीज़ आई?
इन घटनाओं को जानने और स्वीकार करने के बाद यह सवाल उठाना बेहद जायज़ है कि आखिर क्यों कोई फ़िल्मकार, कोई लेखक, कोई निर्देशक इन विषयों पर फिल्म नहीं बनाता? क्या उनका ‘रचनात्मक विवेक’ सिर्फ एक धर्म विशेष के खिलाफ जागृत होता है?
डर किसका है? दबाव किसका है?
जब भी कोई गैर-हिंदू धर्म से जुड़ी कुरीति या अपराध की बात होती है, तब या तो उसे ‘साम्प्रदायिक’ बता कर दबा दिया जाता है या ‘धार्मिक भावनाएँ आहत’ न हों इसलिए उस पर चुप्पी साध ली जाती है। वहीं दूसरी ओर, सनातन धर्म से जुड़ा कोई भी प्रसंग तुरंत आलोचना का पात्र बन जाता है, और उस पर फिल्म, वेब सीरीज़ या लेख आ जाते हैं।
यह दोहरा रवैया ही भारत की सामाजिक सोच और राजनीतिक विमर्श को खोखला बना रहा है। ये वही भारत है जहां एक समय में संतों की वाणी से समाज जागृत होता था, आज वही संत किसी वेब सीरीज़ में बलात्कारी बाबा बनकर सामने आते हैं।
हम यह नहीं कहते कि सनातन धर्म में सब कुछ सही है – बिल्कुल नहीं। जहाँ गलत है, वहाँ बदलाव ज़रूरी है। लेकिन यह बदलाव सभी धर्मों के लिए समान होना चाहिए। सुधार का काम ‘चयनित लक्ष्यों’ पर नहीं, पूरे समाज पर होना चाहिए।
बॉलीवुड – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या एकपक्षीय एजेंडा?
भारतीय संविधान हमें अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। लेकिन यह स्वतंत्रता किसी की धार्मिक भावना को बार-बार ठेस पहुंचाने का लाइसेंस नहीं है। यदि एक वर्ग के विरुद्ध बार-बार फिल्मों, संवादों और व्यंग्य के माध्यम से दुष्प्रचार हो, और बाकी धर्मों पर मौन बना रहे, तो यह कला नहीं, रणनीति है।
यदि किसी फिल्म में मदरसे के अंदर हो रहे कुकृत्य को दिखाने का साहस नहीं है, यदि चर्च में बच्चों के साथ हो रहे बलात्कारों पर कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती, यदि गुरुद्वारों में जातीय भेदभाव या हिंसा पर कोई निर्देशक चुप है – तो यह प्रश्न उठाना लाज़मी है: क्या यह डर है या पक्षपात?
धार्मिक समभाव: संविधान की आत्मा
भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में धर्मों के प्रति समभाव न केवल संविधान की मूल भावना है, बल्कि समाज की एकता का आधार भी है। जब तक धर्मों के बीच तुलनात्मक आलोचना नहीं होगी, तब तक धर्मों में ‘सुधार’ नहीं, बल्कि ‘प्रहार’ होगा।
सनातन धर्म हजारों वर्षों की परीक्षा से निकला हुआ दर्शन है। इसमें आत्मशुद्धि, आत्मनिरीक्षण और परंपरा का विकास हमेशा जारी रहा है। लेकिन जब कोई इसे केवल ‘बुराइयों का केंद्र’ बना कर चित्रित करता है, तो वह केवल एक धर्म का नहीं, भारत की आत्मा का अपमान करता है।
निष्कर्ष: संतुलन ज़रूरी है, नहीं तो विश्वास बिखरेगा
बदलाव चाहिए – लेकिन निष्पक्षता के साथ। अगर समाज को वाकई सुधारना है, तो हमें सब तरफ देखना होगा। सुधार की लौ अगर सिर्फ एक ही दिशा में जलाई जाएगी, तो बाकी अंधेरे में सड़ांध फैलेगी।
बॉलीवुड को, लेखकों को, और समाज को यह समझना होगा कि आस्था केवल मूर्तियों और मंदिरों तक सीमित नहीं होती – वह लोगों के दिलों में होती है, और उसे ठेस पहुँचाना संविधान और नैतिकता दोनों के विरुद्ध है।
अब समय आ गया है कि हम यह प्रश्न करें – क्या हम वाकई एक धर्मनिरपेक्ष समाज में जी रहे हैं, या केवल एक धर्म को निशाना बना कर बाकी को स्वछंदता दे रहे?