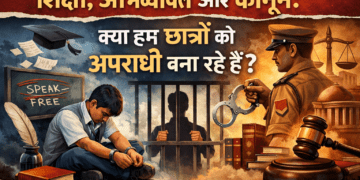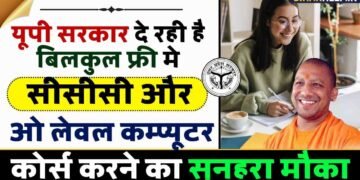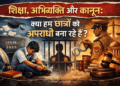वैसे तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है फिर भी आजकल एक नया चलन बन गया है कि जैसे ही कोई नेता या तथाकथित समाज सुधारक बोलना शुरू करता है, तुरंत हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा कर देता है क्युकी ये धर्म सहिष्णुता से भरा है, विरोधी भी बहुत है तो तुरंत लाइम लाइट में आ जाते है और जान से मारे जाने का भी कोई डर नहीं है । अभी हाल ही में पहले गंगवार ने कविता कहकर प्रसिद्धि पा ली तो सपा सांसद रामजीलाल सुमन कैसे पीछे रहते है इनको भी एक गजब का बयान दे दिया की “जब तक हिंदू धर्म में नहीं आएगी समानता, तब तक धर्मांतरण को कोई नहीं रोक सकता” भी उसी मानसिकता का उदाहरण है। लेकिन सवाल यह है – समानता का पैमाना आखिर कौन तय करेगा?
क्या समानता का मतलब यह है कि कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाए और खुद की कमियों को न देखे?
क्या नेता अपने ही घर में समानता निभाते हैं?
अगर समानता की कसौटी पर कसना है तो पहले राजनीति से ही उदाहरण देख लीजिए –
- क्या अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव को जितना सम्मान देते हैं, उतना ही सम्मान शिवपाल यादव या रामगोपाल यादव को भी मिला?
- क्या समाजवादी पार्टी लोहे के समान ‘लोहिया’ को उतनी ही जगह देती है जितनी जगह वह अपने परिवारवाद को देती है?
- क्या दलित आंदोलनकारियों ने बाबा साहब अंबेडकर का नाम जितने सम्मान से लिया, उतने ही सम्मान से बी.एन. राव का नाम लिया, जिन्होंने भारतीय संविधान के ड्राफ्ट में अहम भूमिका निभाई?
जब खुद अपने गुट में ही समानता नहीं निभा पाते तो समाज से किस मुंह से समानता की उम्मीद करते हैं? समानता आखिर किन पैमानों पर चाहिए ? आप मोबाइल चला रहे हो, ट्रेन से लेकर हवाई जहाज में बैठ रहे हो, शिक्षा ले रहे हो, अधिकारी रहे हो, क्या है जो समानता में चाहिए ? वही दूसरी तरफ समानता चाहिए किससे ? सवर्णो से ? तो पहले उनको भी फीस में छूट दो, आयु में छूट दो नंबरों में छूट दो ये उनको है नहीं तो समानता तो वास्तव में सवर्णो को चाहिए और फिर एक रोना की मंदिर में नहीं घुसने देते घर गंगाजल से साफ़ करवाया, मंदिर भगवान का है नहीं जाने देते खुद बनवा लो जैसे उन्होंने बनवाया जो आपको नहीं जाने देते लेकिन बनवाये तो तब जब मन में श्रद्धा हो. मन में बस घृणा है द्वेष है और जबरजस्ती घुसना है भले ही कोई मतलब न हो, उदाहरण अम्बेडकर ने एक मंदिर और एक तालाब में जबरजस्ती घुस कर शक्ति प्रदर्शन किया तो गुस्से में सवर्णो ने उस मंदिर और तालाब को छोड़ दिया, तो फिर दलितों ने क्यों नहीं उस मंदिर और तालाब का सही से देखभाल करके दिखा दिया की हम सिर्फ मांगते ही नहीं वल्कि चीजों को संभालना भी जानते है, लेकिन उद्देस्य तो सिर्फ ये था की चीजे कैसे बर्बाद हो और तालाब और मंदिर दोनों बर्बाद करवा दिया अब चैन आ गया।
बोलने का अधिकार सिर्फ एक पक्ष को क्यों?
आज दलित और पिछड़े वर्ग से जुड़े कुछ नेता खुलकर गालियां देते हैं –
- “तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार”
- “भूरा बाल साफ करो”
मायावती और लालू यादव के ये नारे कोर्ट में सवाल नहीं बनते, कोई सबूत नहीं मांगा जाता। पर जब कोई सवर्ण या ब्राह्मण अपने सम्मान की रक्षा के लिए दूरी बना ले तो तुरंत उसे “भेदभाव करने वाला” कहा जाता है। ये कैसी समानता है? ये कैसी समानता है की एक वर्ग खुले आम ब्राह्मण और सवर्णो को गालिया दे जातिसूचक शब्द बोल बोल कर और बदले में कोई उनके ही तरीके से उनको सुना दे तो मुकदमा वो भी गैर जमानती तो ऐसे लोगो से कौन मेल जोल करेगा जिसमे इज्जत और जेल जाने हमेशा बना रहता हो।
क्या भेदभाव सिर्फ सवर्ण करते हैं?
सच ये है कि भेदभाव कोई भी कर सकता है और करता है –
- पिछड़े दलितों को नीचा दिखाते हैं।
- दलित आपस में ही महादलित, अति दलित में बंटे हैं।
- पिछड़े वर्ग की राजनीति में यादव, कुर्मी, जाट जैसे जातिगत वर्चस्व साफ नजर आता है।
तो क्या ये सब हिंदू धर्म की वजह से है या इंसानी स्वभाव की वजह से? वास्तव में इसमें धर्म को दोष देना व्यर्थ है, ये व्यक्तिगत स्वभाव है, और दूर क्यों जाए, आर्मी का जवान पुलिस के जवान से ज्यादा सम्मान पाता है समाज में जबकि दोनों ही वर्दीधारी और अशोकस्तम्भ लगाए है टोपी पर, इनमे क्यों है भेदभाव ? आपसे में भी भेदभाव है सेना का जवान खुद को ईमानदार और पुलिस वाले को भ्र्स्ट मानता है जनता भी ? क्या ये असमानता नहीं है ?
मनुस्मृति को दोष देना कितना उचित?
हर बात पर मनुस्मृति का नाम लिया जाता है। सवाल यह है –
- क्या मनुस्मृति को कभी स्वतंत्र भारत की शासन-व्यवस्था में लागू किया गया?
- क्या कभी किसी न्यायालय ने इसे कानूनी ग्रंथ मानकर फैसले सुनाए?
- क्या यह संविधान से ऊपर है?
साफ है, मनुस्मृति सिर्फ बहाना है। दलित राजनीति को हवा देने के लिए इसका नाम लिया जाता है, जबकि यह किसी भी कोर्ट, संसद या संविधान में लागू ही नहीं रही।
इतिहास का गलत फायदा
जब कोई धर्मांतरण करता है तो उसका तर्क होता है – “हमसे भेदभाव हुआ।”
पर सवाल है –
- कब हुआ? किसने किया? किस परिस्थिति में हुआ?
- क्या आज भी वही हालात हैं या हालात बदल चुके हैं?
- और अगर भेदभाव को खत्म करने की कोशिश हो रही है तो धर्मांतरण क्यों?
असल में धर्मांतरण में भी भेदभाव खत्म नहीं होता, बस जाति का नाम बदल जाता है। जो भेदभाव हिंदू समाज में था, वह अन्य धर्मों में भी किसी न किसी रूप में मौजूद है।
फायदे लेने की मानसिकता
आज अगर आरक्षण, सरकारी योजनाएं, छात्रवृत्ति, विशेष अवसर न मिलें तो कई लोग घर पर ही बैठे रहना पसंद करेंगे। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि “हमें समाज ने पढ़ने नहीं दिया।”
लेकिन सच ये है कि जब प्रलोभन नहीं था, तब मेहनत करने की मानसिकता भी नहीं थी। अगर कोई ऊंची जाति में पैदा हुआ तो उसने मेहनत से ज्ञान अर्जित किया, मंदिर, आश्रम, गुरुकुल बनाए। लेकिन अब जो कुछ भी तैयार है, उस पर कब्जा करने के लिए आरक्षण और भेदभाव की राजनीति को हथियार बनाया गया।
समानता या सत्ता की भूख?
आज समानता की बात करने वाले लोग क्या चाहते हैं?
- वे चाहते हैं कि उन्हें विशेष सुविधा भी मिले,
- उन्हें कोई कुछ कह न सके,
- वे किसी को भी गाली दें और कोई जवाब न दे,
- और अगर कोई जवाब दे तो उसे भेदभाव करने वाला कहा जाए।
अगर यही समानता है तो ये समानता नहीं, सत्ता और वर्चस्व की भूख है।
धर्मांतरण से क्या समाधान?
जो लोग कहते हैं “धर्मांतरण ही अंतिम उपाय है”, उन्हें सोचना चाहिए –
- क्या धर्म बदलने से मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है?
- क्या मुसलमानों या ईसाइयों में जाति और ऊंच-नीच नहीं है?
- क्या इस्लाम और चर्च में दलितों को बराबरी का स्थान मिला?
सच तो ये है कि धर्मांतरण से समस्या खत्म नहीं होती, बस नया बंधन बनता है।
हिंदू समाज में सुधार की जरूरत है, पर सुधार का मतलब है सबका आत्मनिरीक्षण, न कि सिर्फ एक वर्ग को दोष देना।
- भेदभाव अगर सवर्ण करे तो गलत है,
- लेकिन अगर दलित और पिछड़े भी भेदभाव करें, गालियां दें, राजनीति करें, तो वह भी उतना ही गलत है।
समानता का असली पैमाना यही है – सबको एक ही नजर से देखना, चाहे वह ब्राह्मण हो, दलित हो या पिछड़ा।
अगर ऐसा नहीं होता, तो धर्मांतरण का नारा सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है, समानता का नहीं।