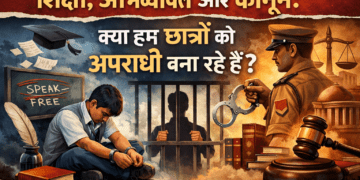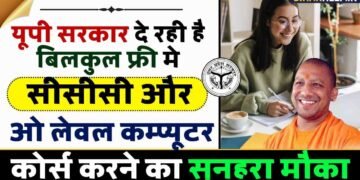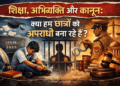जब हम मुफ्त योजनाओं को देखकर वोट देते है तब नहीं सोचते है की आखिर इस मुफ्त की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी
“छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले में एक गर्भवती आदिवासी महिला को उसके पति को 1.5 किलोमीटर तक पीठ पर लादकर अस्पताल पहुँचाना पड़ा क्योंकि पुल टूटा था और एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी।”
यह समाचार मात्र एक दुखद घटना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य तंत्र, राजनीतिक संवेदनशीलता, मीडिया की नीयत और सामाजिक मानवता — इन सबकी सामूहिक विफलता का जीवंत चित्र है।
लेकिन इस दृश्य से भी अधिक भयावह है वह प्रश्न जो इस 52 सेकंड के HD वीडियो को देखकर मन में आता है —
क्या कैमरा सबसे पहले पहुंचा या मदद?
क्या कोई मनुष्य वहाँ पहले था या व्यूज बटोरता यूट्यूबर?
कैमरा पहले, करुणा बाद में?
जब एक व्यक्ति किसी संकट में होता है — जैसे प्रसव पीड़ा से जूझती महिला — तब एक सभ्य समाज का धर्म होता है मदद करना, न कि फ़्रेम सेट करना।
लेकिन यहाँ HD क्वालिटी वीडियो, एंगल से तैयार किया गया दृश्य और पूरा 1.5 KM तक शूट किया गया क्लिप इस बात का प्रमाण है कि मदद से पहले वीडियो बनाने वाला मौजूद था।
कहीं न कहीं यह सवाल उठता है —
क्या वीडियो बनाने वाले को ज़रा भी पीड़ा नहीं हुई उस महिला की कराह सुनकर?
शायद नहीं — क्योंकि संवेदना से ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है ‘Content’ बनाना।
वह भी ऐसा कंटेंट जो भावनाएं भड़काए, भले ही पीड़ित मरता रहे।
सरकारें: चुनाव से पहले आंखें खुलती हैं, बाद में योजनाएं बंद
सत्ताधारी दल के नेता अक्सर कहते हैं — “हमने गांव-गांव तक सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुंचा दीं।”
पर जब जमीनी सच्चाई यह है कि एक गर्भवती महिला को पीठ पर ढोकर ले जाना पड़े, तो क्या यह ‘अमृतकाल’ की अमानवीय तस्वीर नहीं?
सरकारें बुलेट ट्रेन की बात करती हैं, लेकिन गांव में टूटा पुल सालों से नहीं बना।
सरकारें AIIMS और हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की स्कीम गिनाती हैं, लेकिन यहाँ 1.5 KM तक पैदल चलना पड़ता है — वो भी प्रसव की हालत में।
तो प्रश्न है —
क्या आदिवासी क्षेत्रों की महिलाएं ‘भारत माता’ की संतान नहीं हैं?
विपक्ष: विफलता पर राजनीति, समाधान पर चुप्पी
जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो विपक्ष का चेहरा भी सामने आता है —
ट्विटर पर बयानबाज़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आक्रोश, और मंचों पर चीख-चीखकर आरोप।
लेकिन प्रश्न यह है —
जब आप सत्ता में थे, तो क्या आपने वह पुल बनवाया?
क्या आपने उस गांव में PHC या सड़क दी?
क्या आपने ऐसी महिलाओं के लिए कोई स्थायी समाधान खोजा?
नहीं।
क्योंकि विपक्ष भी जानता है कि लोगों की पीड़ा नहीं, उनके वोट मायने रखते हैं।
मीडिया: खबर नहीं, तमाशा चाहिए
मीडिया अब जन-सेवा नहीं करता, वो जन-भावनाओं से खेलता है।
हर चैनल चाहता है:
- दर्द दिखाओ, पर ज़ख्म पर मरहम मत लगाओ
- आँसू दिखाओ, पर आँसुओं को पोंछने वाला मत बनो
- मदद नहीं, ‘Breaking News’ चाहिए
“Exclusive Footage: देखिए कैसे गर्भवती को उठाकर पति चल पड़ा अस्पताल!”
क्या कभी सोचा है कि जिसने 1.5 KM तक वीडियो शूट किया,
वो महिला को स्ट्रेचर देने, कंधा देने, या पीने का पानी देने भी आगे आया था?
नहीं। क्योंकि TRP में इंसानियत नहीं बिकती, ड्रामा बिकता है।
“वीडियो वीर”: जब मोबाइल हाथ में हो, तो दिल मर जाता है
ये जो लोकल रिपोर्टर, यूट्यूबर, सोशल वॉरियर्स हैं —
ये वो लोग हैं जो कष्ट को कला में बदलते हैं।
कष्ट क्लिप बन जाता है
और इंसानियत डिस्क्रिप्शन में कहीं दबी रह जाती है।
“देखिए, महिला को पीठ पर लेकर पति जा रहा है”
— इस वाक्य में साहस नहीं, सिस्टम की लाचारी और समाज की संवेदनहीनता है।
कहाँ गई संवेदना?
क्या हमारे भीतर से “तुरंत मदद” की भावना अब निकल चुकी है?
क्या अब हम हर घटना को “Instagram Reel Opportunity” समझने लगे हैं?
जिस समाज में क्लिक ज़रूरी हो गया हो, और करुणा दुर्लभ, वहाँ फिर सरकार की आलोचना करना आसान हो जाता है — लेकिन आईना खुद को भी देखना चाहिए।
निष्कर्ष: समस्या सत्ता की नहीं, सोच की है
- सरकारें बदलती हैं, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य ढाँचा नहीं बदलता
- विपक्ष बदलता है, लेकिन जनकल्याण की योजनाएं नहीं टिकतीं
- मीडिया के चेहरे बदलते हैं, लेकिन मुद्दों की बाज़ारू प्रस्तुति नहीं बदलती
- और समाज… वह तो वीडियो बनाने में ही अपने कर्तव्य को पूर्ण मानने लगा है
“वीडियो बनाने से समाज नहीं बदलता, हाथ बढ़ाने से बदलता है।
क्लिप काटने से न्याय नहीं होता, करुणा दिखाने से होता है।”
आइए — मिलकर ये प्रण लें:
अगली बार अगर किसी को पीड़ा में देखें —
तो कैमरा नहीं, कंधा आगे करें।