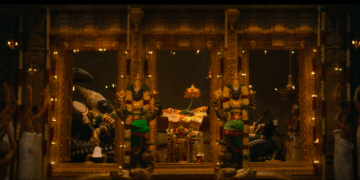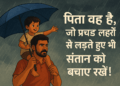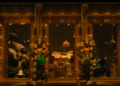सिनेमा समाज का आईना होता है। यह न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि सामाजिक सोच, संवेदनाओं और परिवर्तन का भी एक शक्तिशाली उपकरण है। हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म “फुले” के कलेक्शन ने इस बात को साफ़ कर दिया है कि अब भारत में नफरत फैलाने वाली, खासकर जातिगत द्वेष को बढ़ावा देने वाली फिल्मों का दौर खत्म होता जा रहा है। जहां एक ओर फुले जैसी संतुलित और तथ्य-आधारित फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट हो गया कि अब जनता भावनाओं के शोषण से थक चुकी है।
फुले फिल्म का कलेक्शन
फिल्म “फुले” को बड़े स्तर पर प्रचार मिला, इसे एक “क्रांतिकारी” फिल्म के तौर पर प्रस्तुत किया गया जो ‘जातिगत अन्याय’ के खिलाफ आवाज़ उठाती है। लेकिन जब बात बॉक्स ऑफिस पर सफलता की आई, तो यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। पहले हफ्ते में इसका कुल कलेक्शन मात्र 8 से 9 करोड़ रुपये के बीच रहा, जबकि इसकी लागत इससे कहीं ज्यादा थी। यह आंकड़ा साफ़ इशारा करता है कि दर्शकों ने इस फिल्म को नकार दिया।
दर्शकों की बदलती सोच
एक दौर था जब दो बीघा ज़मीन, मदर इंडिया, शूद्र जैसी फिल्में जातिगत संघर्ष और पीड़ा को इस तरह दिखाती थीं कि एक पक्ष को पूरी तरह से खलनायक बना दिया जाता था। तब ऐसी फिल्मों को न केवल प्रशंसा मिलती थी, बल्कि अवार्ड्स भी दिए जाते थे। लेकिन आज का दर्शक केवल सहानुभूति या गुस्से की बिक्री को नहीं स्वीकार करता।
अब आम जनता यह समझने लगी है कि जातिगत द्वेष दिखाने वाली फिल्में एक एजेंडा के तहत बनाई जाती हैं — उनका उद्देश्य सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि भावनात्मक शोषण और राजनीतिक लाभ होता है। जब किसी समाज के भीतर बार-बार एक वर्ग को ‘दोषी’ बताकर प्रस्तुत किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से दूसरे वर्ग में भी असुरक्षा और द्वेष की भावना जन्म लेती है। यह सामाजिक एकता को तोड़ने वाला काम है, जो लंबे समय में पूरे राष्ट्र को कमजोर करता है।
सामाजिक परिणाम: एकता में दरार
फिल्में जो बार-बार सवर्ण समुदाय को उत्पीड़क की भूमिका में दिखाती हैं, वे यह भूल जाती हैं कि वास्तविकता में आज भी देश भर में लाखों सवर्ण लोग बिना किसी भेदभाव के सेवा, सहायता और भाईचारे की भावना से काम करते हैं। लेकिन जब बार-बार उन्हें अपमानित और कलंकित किया जाता है, तो वे स्वाभाविक रूप से अपने कदम पीछे खींच लेते हैं।
जो लोग पहले हर मुश्किल समय में मदद के लिए आगे आते थे, वे अब यह सोचने लगे हैं कि उनकी सहानुभूति का बदला उन्हें घृणा और नफरत के रूप में क्यों मिल रहा है। यही कारण है कि समाज में वर्गों के बीच जो प्राकृतिक सहयोग था, वह अब टूटने लगा है।
जनता का नया संदेश
फुले फिल्म के कलेक्शन ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अब जनता उन फिल्मों को महत्व नहीं देगी जो किसी भी वर्ग को विलेन बनाकर नफरत फैलाने की कोशिश करेंगी। दर्शकों को अब यह समझ आ चुका है कि बहुत बार ये फिल्में राजनीतिक या वैचारिक फायदे के लिए बनाई जाती हैं, और इनका मकसद समाज को बांटना होता है।
आज का युवा वर्ग शिक्षा, तकनीक और वैश्विक सोच से लैस है। वह जाति से ऊपर उठकर सोचता है और यही सोच अब सिनेमा में भी दिख रही है।
निष्कर्ष
फुले फिल्म का असफल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन केवल एक फिल्म की विफलता नहीं, बल्कि एक मानसिकता की पराजय है जो अब प्रासंगिक नहीं रही। भारत की जनता अब वह दौर पीछे छोड़ चुकी है जब जातिगत द्वेष पर आधारित कहानियों को आँख बंद करके सराहा जाता था।
अब सिनेमा में भी वैसी ही कहानियाँ चलेंगी जो सामाजिक एकता, न्याय और समानता को आगे बढ़ाएं — न कि ऐसे विषय जो पुराने जख्मों को कुरेदकर समाज को फिर से बाँटने का काम करें। फुले फिल्म की विफलता इस बात का संकेत है कि अब नफरत नहीं, समरसता ही सफल होगी।