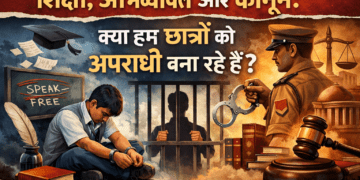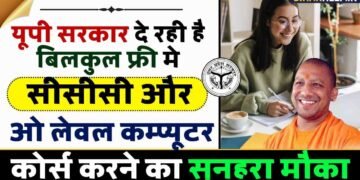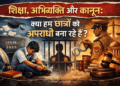भारत में जाति और वर्ण की चर्चा करते समय अक्सर “मनुस्मृति” को कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन क्या किसी ने यह सवाल उठाया है कि मनुस्मृति की जो वर्ण व्यवस्था थी, उसमें व्यक्ति का वर्ण उसके कर्म से बदलता था, जबकि आज का संविधान जाति को जन्म से जोड़ता है?
यह एक ऐसा तथ्यात्मक और चिंतनीय विरोधाभास है, जिस पर विचार किए बिना हम न्याय, समानता और अवसर की वास्तविक बात नहीं कर सकते।
संविधान और जाति की जन्म आधारित परिभाषा
आज भारत का शासन संविधान से चलता है, न कि किसी पुरातन ग्रंथ से।
लेकिन क्या संविधान ने जाति और सामाजिक विभाजन को मिटाया?
नहीं। उल्टा उसे स्थायी कर दिया।
आज आप एक IAS अधिकारी बन जाएँ, राष्ट्रपति भी बन जाएँ, लेकिन आपकी जाति आपके साथ चलेगी।
आप “मैं सिर्फ एक राष्ट्राध्यक्ष हूँ” नहीं कह सकते।
टीना डाबी हो या महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी — समाज और मीडिया कहेगा:
“ये हमारी जाति की हैं।”
यानि आज का सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि जाति आपकी पहचान से चिपकी रहे, भले आप कितने भी ऊँचे पद पर क्यों न पहुँचें।
समाज की परंपरा: आस्था आधारित मूल्यांकन
वहीं दूसरी ओर, हमारा सनातनी समाज एक अलग नजरिए से लोगों को परखता रहा है।
- इस समाज ने कभी कालनेमि, रावण, राहु, ब्रह्मा और इंद्र तक की पूजा नहीं की — भले वो शक्तिशाली थे, लेकिन उनका आचरण संदेहास्पद या छलपूर्वक था।
- वहीं, कबीर, रविदास, रहीम — जो ईश्वरभक्ति और सत्य के मार्ग पर रहे — उन्हें पूरे सम्मान से स्वीकारा।
यह समाज देखता था कि कोई कौन है, ये मायने नहीं रखता – वो क्या कर रहा है, किसकी भक्ति में है, वही मायने रखता है।
सरकारी सिस्टम: सिर्फ जन्म देखता है, जीवन नहीं
अब ज़रा इस उदाहरण पर ध्यान दीजिए:
- एक सवर्ण युवक, जो 45 साल की उम्र तक बेरोजगार रहा।
- उसके पास धन नहीं, समाज का सहयोग नहीं, कोई सहारा नहीं।
- परिवार ने उपेक्षा कर दी, शादी नहीं हुई, समाज से कट चुका है।
अगर वह युवक अपनी दशा से मजबूर होकर आरक्षित वर्ग का प्रमाणपत्र बनाकर नौकरी पा ले, तो?
10 साल बाद सरकार को पता चलता है कि वह “सवर्ण” था —
तो क्या सरकार यह देखेगी कि:
“वो आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़ा था, इसलिए उसने किया”?
नहीं।
सरकार कहेगी – “धोखाधड़ी हुई है।”
उसे जेल होगी, नौकरी से बर्खास्तगी होगी, और जुर्माना भी लगेगा।
यानि वास्तविक पीड़ा नहीं देखी जाएगी, देखा जाएगा सिर्फ जन्म।
तो बताइए — क्या यही है न्याय?
धर्म की आड़ में पहचान छुपाना: समाज कब बर्दाश्त नहीं करता
हाल ही में उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के दंदरपुर गांव में ऐसी ही एक घटना घटी।
एक मुकुटमणि यादव, मुकुटमणि अग्निहोत्री बनकर कथा कर रहे थे।
वे ब्राह्मण नाम से आए — कथा करने के लिए अग्रिम राशि भी ली गई।
किंतु बीच कथा में ही जब श्रोताओं ने कुछ ऐसा देखा, जो ब्राह्मणोचित नहीं था, तो उनकी वास्तविक पहचान सामने आई।
👉 अब सवाल ये है कि क्यों पकड़ा गया?
क्या उन्होंने कथा बुरी की?
नहीं।
लेकिन उन्होंने अपनी वास्तविक जाति छुपाई, और धर्म की आड़ में आस्था से खिलवाड़ किया।
यदि वे “मुकुटमणि यादव” नाम से ही कथा करते, और फिर उनके साथ दुर्व्यवहार होता — तो वह निंदनीय होता।
लेकिन पहचान छुपाकर, ब्राह्मण उपनाम लगाकर कथा करना — ये जनविश्वास का छल है।
समाज कभी भी छल को सम्मान नहीं देता — चाहे वो राजा हो या कथावाचक।
निष्कर्ष: दोहरा मापदंड क्यों?
- जब धर्मग्रंथों की व्यवस्थाओं को “पुराने ज़माने की चीज़” बताकर खारिज किया जाता है,
- लेकिन उसी breath में आज का संविधान जन्म आधारित जाति व्यवस्था बनाए रखता है,
- तो यह एक बौद्धिक पाखंड है, न्याय का उपहास है।
आज की “प्रगतिशील” व्यवस्था में भी कोई भी सामाजिक-सांस्कृतिक न्याय नहीं है।
जाति अब कर्म से नहीं बदलती।
जाति अब आचरण से नहीं बनती।
जाति अब समाज के अनुभव से नहीं, सिर्फ प्रमाणपत्र से बनती है।
अंतिम बात:
सनातन समाज ने हमेशा सत्य को देखा, आस्था को प्राथमिकता दी, और आचरण को मापदंड माना।
आज के सिस्टम ने जन्म और प्रमाणपत्र को धर्म, नीति और न्याय से ऊपर रख दिया है।
जब तक हम इस असंतुलन को नहीं पहचानेंगे,
तब तक ना जातीय भेद मिटेगा, ना सामाजिक न्याय स्थापित होगा।