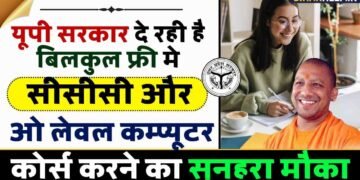शनिवार, 23 अगस्त 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने गोवा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में कहा कि –
“समानता का मतलब सभी के साथ एकसमान व्यवहार करना नहीं है। संविधान असमानता को समान बनाने के लिए असमान व्यवहार की वकालत करता है।”
यह कथन सुनने में जितना तर्कसंगत और दार्शनिक लगता है, उतना ही गहरे सवाल खड़े करता है। आखिर संविधान की वह मूल आत्मा, जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत “कानून के समक्ष समानता” और “कानून द्वारा समान संरक्षण” की गारंटी देती है, वह आज किस दिशा में ढल चुकी है?
समानता या चयनात्मक समानता?
अनुच्छेद 14 का आशय था – जाति, धर्म, लिंग या वर्ग की परवाह किए बिना हर भारतीय को समान अवसर और समान अधिकार मिले। लेकिन जब देश का सर्वोच्च न्यायिक पद यह कहे कि “समानता का मतलब समान व्यवहार नहीं”, तो सामान्य वर्ग के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि – क्या वास्तव में उन्हें संविधान में बराबरी का दर्जा मिला भी है?
आज स्थिति यह है कि सामान्य वर्ग का नागरिक यह मानकर चलता है कि “कानून सबके लिए समान है”, लेकिन न्यायपालिका स्वयं यह स्वीकार कर रही है कि असमानता को दूर करने के नाम पर जानबूझकर असमान व्यवहार किया जाएगा। यह सीधा संकेत है कि सामान्य वर्ग को बराबरी का हक नहीं, बल्कि उनके साथ “भेदभाव” ही एक संवैधानिक नीति है।
असमानता का सबसे बड़ा उदाहरण – आरक्षण और विशेष कानून
भारत में आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई थी सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों को अवसर देने के लिए। लेकिन धीरे-धीरे यह व्यवस्था एक “स्थायी राजनीतिक औजार” बन गई।
- आज सामान्य वर्ग का एक योग्य छात्र केवल इसलिए अवसर से वंचित हो जाता है क्योंकि उसका जन्म किसी विशेष जाति में नहीं हुआ।
- सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों और छात्रवृत्तियों तक में उसकी राहें बंद कर दी जाती हैं।
- यहाँ तक कि कई बार यह कहा जाने लगा है कि “सामान्य वर्ग तो पहले से ही सक्षम है”, जबकि गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी उसी वर्ग में भी व्यापक रूप से मौजूद है।
यह कैसी समानता है जहाँ “सिर्फ जाति” के आधार पर विशेषाधिकार और अधिकारों का बंटवारा हो रहा है?
SC/ST एक्ट – न्याय या अन्याय?
सवर्ण समाज के लिए सबसे बड़ा दर्दनाक अनुभव है – अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act)।
- इस कानून के अंतर्गत यदि कोई अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति किसी सवर्ण पर आरोप लगा दे, तो तुरंत गिरफ्तारी, तुरंत केस दर्ज और लंबे मुकदमे का सामना – यही प्रक्रिया है।
- अगर बाद में मामला झूठा साबित हो जाए, तो न तो आरोप लगाने वाले को कोई सजा होती है और न ही दिए गए सरकारी मुआवजे की कोई वापसी होती है।
- कई बार इसका दुरुपयोग कर सवर्ण परिवार की महिलाओं तक को ब्लैकमेल किया गया है।
सवाल यह है कि क्या यह न्याय है? या यह सामान्य वर्ग को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की सोची-समझी रणनीति है?
लोकतंत्र और समाजवाद – सिर्फ़ नारों तक सीमित
भारतीय संविधान में लोकतंत्र और समाजवाद की नींव रखी गई थी। परंतु आज यह दोनों शब्द केवल खोखले नारे बन चुके हैं।
- लोकतंत्र का मतलब सबकी आवाज़ सुनी जाए, लेकिन सामान्य वर्ग की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं।
- समाजवाद का मतलब अवसरों का न्यायपूर्ण बंटवारा हो, लेकिन व्यवहार में यह “राजनीतिक वोटबैंक” तक सिमट कर रह गया है।
- यदि कोई वकील या नागरिक इस असमानता पर सवाल उठाता है, तो “कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट” (अवमानना) का डर दिखाकर उसकी आवाज दबा दी जाती है।
तो क्या लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा है, जहाँ बहुसंख्यक वर्ग को ही हाशिये पर डाल दिया जाए?
मुख्य न्यायाधीश का कथन और उसका प्रभाव
जब देश का मुख्य न्यायाधीश यह कहे कि “समानता का मतलब समान व्यवहार नहीं”, तो यह केवल एक टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि न्यायपालिका भी अब इस असमानता की पक्षधर बन चुकी है। इससे यह संदेश जाता है कि –
- सवर्ण वर्ग को न तो न्यायपालिका से कोई विशेष उम्मीद रखनी चाहिए।
- न ही यह सोचना चाहिए कि संविधान उन्हें समान अधिकार देता है।
- बल्कि उन्हें यह मान लेना चाहिए कि उनकी स्थिति “कीड़े-मकोड़ों” से अधिक नहीं, जिन्हें जब चाहे कानून के नाम पर कुचल दिया जाए।
अगर संविधान ही असमानता को जायज़ ठहराए तो…?
अब सवाल यह उठता है कि अगर संविधान ही असमानता की वकालत करता है, तो फिर इस संविधान की नैतिक वैधता क्या रह जाती है?
- क्या इसे “लोकतांत्रिक संविधान” कहा जा सकता है?
- क्या इसे “समाजवादी व्यवस्था” माना जा सकता है?
- या फिर यह महज एक “राजनीतिक दस्तावेज़” है, जिसका इस्तेमाल केवल विशेष वर्गों के लिए विशेषाधिकार सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है?
यदि वास्तव में यही स्थिति है, तो संविधान का नाम ही बदल देना चाहिए। ताकि कम से कम सामान्य वर्ग इस भ्रम में न रहे कि यह देश “सबके लिए समान” है।
सवर्ण वर्ग की पीड़ा और भविष्य की दिशा
सामान्य वर्ग का सबसे बड़ा दर्द यह है कि –
- वह कर चुकाता है, लेकिन सुविधाएँ दूसरों को मिलती हैं।
- वह कानून का पालन करता है, लेकिन उसी कानून के तहत उसे बार-बार दोषी ठहराया जाता है।
- वह राष्ट्रनिर्माण की रीढ़ है, लेकिन उसका योगदान ही नकारा जाता है।
ऐसी स्थिति में सवाल उठना लाजमी है कि – क्या सवर्ण वर्ग को इस लोकतांत्रिक और समाजवादी देश में जीने का अधिकार है भी या नहीं?
निष्कर्ष
भारत का संविधान समानता का दावा करता है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर यह “चयनात्मक समानता” का पक्षधर बन चुका है। जब देश का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी ही इस बात को खुलकर कह दे कि “समानता का मतलब समान व्यवहार नहीं”, तो सामान्य वर्ग को यह समझ लेना चाहिए कि उनकी बराबरी का सपना केवल छलावा है।
आज जरूरत है कि –
- इस “चयनात्मक समानता” के खिलाफ आवाज उठे।
- संविधान और कानून की असली आत्मा – यानी सबके लिए न्याय और सबके लिए समान अवसर – की ओर वापसी हो।
- अन्यथा आने वाली पीढ़ियाँ इस भ्रम में न जीएँ कि वे एक लोकतांत्रिक और समानतावादी देश में हैं।
यदि असमानता ही संवैधानिक सिद्धांत है, तो बेहतर है कि संविधान को “लोकतंत्र का प्रतीक” कहकर पूजना बंद कर दिया जाए और उसकी असली पहचान को उजागर किया जाए।