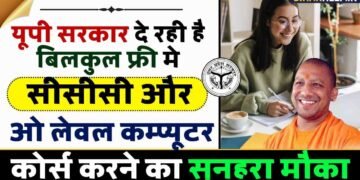आज के तथाकथित आधुनिक विमर्श में “वर्ण‑व्यवस्था” का नाम लेते ही मानो कोई अदृश्य हथौड़ा ब्राह्मणों और सनातन संस्कृति पर बरस पड़ता है। मीडिया की सुर्खियाँ, वामपंथी अकादमिक भाषण और सोशल‑मीडिया के ट्रेंड एक ही राग अलापते हैं—“ब्राह्मणों ने शूद्रों को दबाया, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा, मंदिरों से दूर रखा।” पर क्या यही सम्पूर्ण सत्य है? क्या प्राचीन भारत सचमुच ‘जातीय उत्पीड़न’ की प्रतीक भूमि था, या यह सब हमारे वर्तमान राजनीतिक स्वार्थों की धुंध से उपजा भ्रम है? आइए, इतिहास, शास्त्र और तर्क—तीनों की रोशनी में इस प्रश्न का निष्पक्ष विश्लेषण करें।
1. शास्त्रीय मूल—गुण‑कर्म आधारित सामाजिक इंजीनियरिंग
भगवद्गीता (4.13) का सुप्रसिद्ध श्लोक चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः न केवल दैवी उद्घोष है, बल्कि प्राचीन भारतीय समाज‑विज्ञान का सार भी है।
- गुण = व्यक्तिगत स्वभाव, मानसिक प्रवृति, आध्यात्मिक झुकाव।
- कर्म = वह कार्य जिसे व्यक्ति स्वेच्छा से या पारिवारिक परम्परा से चुनता है।
इन दो कसौटियों पर खरे उतरकर ही कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बनता था। जन्म मात्र निर्णायक नहीं था; यही कारण है कि महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में जन्में और ब्रह्मर्षि बने, जबकि रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी राक्षस चरित्र का प्रतीक हुआ।
2. वर्ण व्यवस्था एक मर्यादा है अपमान नहीं
इसे समझने के लिए एक आधुनिक रूपक देखिए। एक उच्च स्तरीय मेडिकल कॉन्फ़्रेंस में सिर्फ़ डॉक्टर‑सर्जन ही वक्ता बनते हैं, जबकि आयोजन स्थल पर सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर, हाउसकीपिंग स्टाफ सम्मान सहित बाहर इंतज़ार करते हैं। क्या यह ‘सुरक्षाकर्मी‑विरोधी’ भेदभाव है? नहीं—यह कार्य विशेषता और मर्यादा का अनुशासन है।
इसी प्रकार:
- ब्राह्मण = यज्ञ, वेदाध्ययन, शिक्षा‑दर्शन का दायित्व।
- क्षत्रिय = राज्य‑सुरक्षा, न्याय, प्रशासन का दायित्व।
- वैश्य = कृषि, व्यापार, अर्थविज्ञान का दायित्व।
- शूद्र = सृजन, सेवा, कला‑कारीगरी का दायित्व।
हर वर्ण सामाजिक ताने‑बाने का अनिवार्य स्तंभ था—हीन नहीं, विशिष्ट।
3. शूद्र एक अपार कौशल का कोश
मनुस्मृति (1.91‑93) कहती है—“शूद्र शब्द सेवा‑परिचर्या तक सीमित नहीं; वह समाज रचना की वहन‑शक्ति है।”
- विश्वविख्यात मूर्तिकला (अजन्ता‑एलोरा),
- नक्काशी‑कारी शिल्प‑शास्त्र (विश्वकर्मा परंपरा),
- सुरीली संगीत परंपरा—ये सब मुख्यतः शूद्र और विषयकुल कलाकारों के हस्ताक्षर थे।
विदुर, कुण्डी‑पुत्र निषादराज गुह, आहिल्या शिल्पकार कुल, कुंभकार श्रेष्ठी—ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारत में श्रमशील वर्ग सामाजिक रीढ़ था, जैसा आज के इंजीनियर या तकनीशियन।
4. भ्रांतियाँ कैसे जन्मीं?—मध्यकालीन विकृति
मुग़ल आक्रमण, फिर औपनिवेशिक सत्ता के दौरान राजनीतिक‑सामाजिक उथल‑पुथल ने वर्ण‑व्यवस्था को जन्माधारित सीढ़ी में ढक दिया। शिक्षा के प्राचीन गुरुकुल उजड़ गए; आर्थिक संसाधन लूटे गए; और ब्रिटिश ‘Divide and Rule’ नीति ने जातीय दरारें चौड़ी कीं। परिणाम:
- कर्म‑गत वर्ण जन्म‑गत जाति में घिसट गया।
- ब्राह्मण ग्रामिण शिक्षा‑केंद्र से राजाश्रित पुजारियों तक सीमित हुए।
- शूद्रों‑वैश्यों की उत्पादनशीलता को विदेशी कर‑नियमों ने तोड़ ‑ मरोड़ दिया।
इन ऐतिहासिक आघातों को अनदेखा कर आज की पॉलिटिकली करेक्ट लॉबी पूर्ण दोष सनातन व्यवस्था पर मढ़ देती है—यह बौद्धिक बेईमानी है।
5. आधुनिक भेदभाव के पर्दे में छुपा एजेंडा
आज ‘जाति‑उन्मूलन’ के नाम पर सक्रिय कई संगठन वास्तव में वोट‑बैंक की खेती करते हैं।
- वे अतीत के चयनित उदाहरणों को बढ़ा‑चढ़ाकर दिखाते हैं ताकि वर्तमान सरकारी नियुक्तियों, ठेकों, वंशवादी राजनीति और माफियागर्दी से ध्यान भटके।
- सोशल‑मीडिया पर ‘ब्राह्मणवाद’ गाली बन जाए, तो नये‑नये आरक्षण‑पैकेज और NGO‑उद्योग निर्विघ्न फलें‑फूलें।
6. शस्त्र और शास्त्र—परशुराम प्रसंग से वस्तुपरक सीख
- भीष्म क्षत्रिय थे, पर धर्मपरायण; अतः परशुराम ने उन्हें शस्त्रविद्या दी।
- कर्ण ने झूठ बोलकर ब्राह्मण कहा, अतः शाप मिला—कर्म दोष पर दंड, जाति पर नहीं।
- द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, पर निपुण शस्त्रगुरु बने—यह गुण‑कर्म सिद्धांत की प्रत्यक्ष मिसाल है।
ये प्रसंग सिद्ध करते हैं कि प्राचीन गुरु योग्यता देखते थे, जन्म नहीं।
7. वर्ण‑व्यवस्था की पुनर्व्याख्या—समकालीन संदर्भ
यदि आज हम IIT‑संधानकर्ता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैनिक, किसान, कारीगर—सभी को समान महत्त्व देते हैं, तो क्या हम “वर्ण” का आधुनिक संस्करण ही नहीं प्रयोग कर रहे? फर्क सिर्फ इतना है कि हमने संस्कृत शब्दावली त्याग दी, पर सिद्धांत—कार्य विभाजन—अब भी यथावत है।
मर्यादा ≠ भेदभाव: सेमिनार‑हॉल का अनुशासन, कोर्ट‑कक्ष की प्रकिया, सैनिक छावनी का अनुक्रम—सभी उसी सामाजिक इंजीनियरिंग के आधुनिक प्रतिबिम्ब हैं।
8. वामपंथी प्रोपेगेंडा का प्रत्युत्तर—पांच तर्कसंगत प्रतिज्ञाएँ
- इतिहास को संपूर्णता में पढ़ें—टुकड़ों में नहीं।
- गुण‑कर्म सिद्धांत को जन्माधारित नहीं ठहराएँ—महर्षियों, ऋषिकाओं और शूद्र महापुरुषों के उदाहरण अन्तहीन हैं।
- वर्तमान शोषण पर बात करें—ठेकेदारी‑भाई‑भतीजावाद पर—not dead ब्राह्मणवाद।
- सामुदायिक सहयोग को पुनर्जीवित करें—कला, कृषि, विज्ञान सबमें सबकी साझेदारी बने।
- धर्म को दोषी ठहराने से पहले धर्म ग्रन्थ पढ़ें—अनुवादित एजेंडा नहीं, मूल संस्कृत।
उपसंहार—कलंक का ध्वंस, मर्यादा का पुनर्स्मरण
वर्ण‑व्यवस्था का मूल विचार सम्मिलित उत्तरदायित्व था, न कि ऊँच‑नीच का अहं। वह सामाजिक सामंजस्य का विज्ञान था, जिसमें हर वर्ण, हर कार्य, हर व्यक्ति—धर्मस्य मूलं इति—की महत्ता स्वीकृत थी। कालगति, विदेशी आक्रमण और राजनैतिक स्वार्थ ने इस व्यवस्था को विकृत किया; उसी विकृति को आज संपूर्ण इतिहास कहकर पेश करना खुद एक बौद्धिक शोषण है।
आज आवश्यकता है कि हम गुण‑कर्म आधारित सम्मान को पुनर्जीवित करें—चाहे वह लैब के वैज्ञानिक हों, खेत का किसान, संगीतकार हो या सफाई‑कर्मी। सनातन दृष्टिकोण यही संदेश देता है:
“स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।”
(अपना कर्तव्य, अपने गुण‑कर्म के अनुरूप निभाना—यही श्रेष्ठ है; दूसरे का अनुकर्ण भयावह।)
जब तक हम इस श्लोक की ज्योति में समाज रचेंगे, तब तक भेदभाव के दावों की धुंध स्वतः छँट जाएगी, और वर्ण‑व्यवस्था की असली रूपरेखा फिर से मर्यादा और सहयोग का दीपक बनकर प्रकाशित होगी।