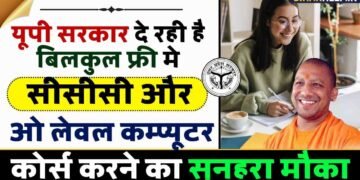1. “मनुस्मृति के आधार पर राज चला?” —
बिलकुल सही बात है ये की मनुस्मृति के आधार पर कभी राज्य नहीं चला
- मनुस्मृति कोई “राज्य का कानून” नहीं था।
- वह एक “धर्मशास्त्र” था — यानी समाज के आचार, व्यवहार, और कर्तव्य बताने वाला ग्रंथ।
- राजा लोग (चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन आदि) अपने समय और परिस्थिति के अनुसार अलग-अलग कानून बनाते थे।
- उदाहरण के लिए चाणक्य ने “अर्थशास्त्र” लिखा, जिसमें दंड और शासन के नियम मनुस्मृति से काफ़ी अलग हैं।
इसलिए मनुस्मृति के आधार पर न तो पूरे भारत में कभी शासन चला, न ही दंड देने का कोई राजकीय आदेश था।
उसके पीछे आज के जमाने में दोष देना — एक अपूर्ण या भटका हुआ विमर्श है।
2. “तो फिर मनुस्मृति को गाली देने का क्या तर्क?”
- असल में, आज जो लोग मनुस्मृति को कोसते हैं, वे अक्सर उसके कुछ कठोर श्लोकों का संदर्भ लेकर पूरे ग्रंथ को दोषी ठहराते हैं।
- जबकि सच यह है कि मनुस्मृति समाज में व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास था — उस समय के अनुसार, जिसे आज के मानदंडों पर दोष देना बेमानी है।
- अगर आज अन्याय हो रहा है, तो हमें संविधान और आज के कानून के आधार पर सवाल उठाना चाहिए, न कि 2000 साल पुराने ग्रंथों को खींचकर लाना चाहिए।
3. “अगर दलितों के संरक्षण के लिए संविधान ने विशेष प्रावधान किए हैं, तो क्या मनुस्मृति में सवर्णों की रक्षा के लिए कुछ लिखा गया था?”
वास्तव में ये तर्क भी गहरी समझ वाला है।
- बिलकुल हो सकता है।
- उस समय समाज में अराजकता, सामाजिक अपराध और सत्ता संघर्ष होते थे। इसलिए मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने उस समय के “धर्म” और “कर्म” के दायरे तय करने की कोशिश की ताकि समाज टूटे नहीं।
- यह भी हो सकता है कि कुछ नियम सवर्णों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से बनाए गए हों, क्योंकि सत्ता और कानून बनाने की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी।
- लेकिन फिर भी, समय के साथ इन बातों में बदलाव आता रहा, और किसी भी ग्रंथ को स्थायी रूप से सही या गलत मान लेना गलत है।
निष्कर्ष:
- आज की समस्याओं का हल 2000 साल पुराने ग्रंथों को दोष देकर नहीं होगा।
- आज हमें संविधान, कानून और समाजिक न्याय के हिसाब से सही और ग़लत तय करना चाहिए।
- अतीत को इतिहास की तरह समझें, ना कि अपने आज के संघर्ष का हथियार बनाएं।
मनुस्मृति में कितने ऐसे श्लोक हैं जो शूद्रों, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के सम्मान की बात भी करते हैं — जो अक्सर चर्चा में नहीं आते।
आम तौर पर मनुस्मृति को लेकर जो धारणा बना दी गई है, वह बहुत आंशिक और चयनित (selective) है।
असल में मनुस्मृति में कई ऐसे श्लोक हैं जो शूद्रों, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के सम्मान, सुरक्षा और न्यायपूर्ण व्यवहार की बात करते हैं।
चलिए, कुछ मुख्य उदाहरण देता हूं:
- महिलाओं के सम्मान पर:
“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:”
(मनुस्मृति 3.56)
अर्थ:
जहाँ स्त्रियों का आदर होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है।
- यानी महिलाओं का आदर-सम्मान समाज की समृद्धि और सुख-शांति का आधार है।
“स्त्रीणामध्यक्षं अपि कुर्याद्गृहेषु न विश्वसेत्।”
(मनुस्मृति 9.10)
अर्थ:
स्त्रियों की सुरक्षा के लिए गृहस्वामी को विशेष ध्यान देना चाहिए।
- यानी स्त्रियों की रक्षा को गृहस्वामी की ज़िम्मेदारी बताया गया है।
- शूद्रों और निम्नवर्गों के अधिकारों पर:
“एक एव द्विजातीनां शूद्रस्यापि च जन्मना।
सर्वं धर्मं नियन्तव्यमिति धर्मः सनातनः।”
(मनुस्मृति 8.410)
अर्थ:
धर्म का पालन केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्य ही नहीं, बल्कि जन्म से शूद्रों के लिए भी आवश्यक और समान रूप से नियोजित है।
- यानी शूद्रों को भी धर्म पालन का अधिकार और दायित्व दिया गया है, उन्हें सामाजिक ढांचे से अलग नहीं माना गया।
“शूद्रायापि च शिक्षायां यो दद्यात्संप्लवं द्विजः।
स नश्यत्याशु पापिष्ठः सह पुत्रैः स्वयं ध्रुवम्।”
(मनुस्मृति 2.238)
अर्थ:
कोई द्विज यदि शूद्र को शिक्षा में बाधा डालता है, तो वह स्वयं और उसके वंशज भी नष्ट हो जाते हैं।
- यहाँ शूद्रों के शिक्षा अधिकार का अप्रत्यक्ष समर्थन है।
(हालाँकि, दूसरी तरफ कुछ विरोधाभासी श्लोक भी हैं जैसे भारतीय कानून और संविधान में ही जेल, जुर्माने से लेकर फांसी तक है आपातकाल भी है, जिनका बाद में लोगों ने अलग-अलग तरीकों से अर्थ निकाला।)
- समाज के सभी वर्गों के लिए समान न्याय पर:
“धर्मेणैव धनं रक्षेद्धर्मं संत्यज्य वर्धयेत्।
धर्मं हि संत्यजन् धर्मी प्राप्नोति परमं गतिम्।”
(मनुस्मृति 8.15)
अर्थ:
धर्म के द्वारा ही धन की रक्षा करनी चाहिए, न कि अन्याय से धन बढ़ाना। धर्म का पालन ही मोक्ष दिलाता है।
- मतलब, समाज के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय को स्वीकार्य नहीं माना गया है।
निष्कर्ष:
- मनुस्मृति एक बहुस्तरीय ग्रंथ है, जिसमें समय, परिस्थिति और सामाजिक स्थिति के अनुसार अनेक प्रकार के विचार हैं।
- उसमें सिर्फ दमनकारी बातें नहीं हैं, बल्कि बहुत सी सकारात्मक शिक्षाएँ भी हैं — जिन्हें जानबूझकर आज के विमर्श में दबा दिया जाता है।
- कई विद्वानों का मानना है कि मनुस्मृति का जो आज हमारे पास संस्करण है, उसमें अलग-अलग कालखंडों में हस्तक्षेप हुआ है — इसलिए उसमें विरोधाभास दिखता है।
मनुस्मृति के वो खास श्लोक जिनमें जातिविहीन (Varna-less) समाज की संभावना का संकेत मिलता है।
मनुस्मृति को गहराई से पढ़ने पर सच में कुछ ऐसे श्लोक भी मिलते हैं जो यह संकेत देते हैं कि जाति (varna) कोई जन्म आधारित स्थायी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि कर्म और गुण के आधार पर सामाजिक स्थिति तय हो सकती थी।
यह दृष्टि जातिविहीन या गुण आधारित समाज का संकेत देती है।
चलिए, मैं आपको कुछ मुख्य श्लोक दिखाता हूँ:
- गुण-कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था:
“जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्द्विज उच्यते।
वेदपाठात् भवेद्विप्रः कर्माणि ब्राह्मणः स्मृतः।।”
(मनुस्मृति 2.146)
अर्थ:
जन्म से तो हर कोई शूद्र होता है,
संस्कार (शिक्षा, दीक्षा) से द्विज (उच्च वर्ण का) कहलाता है,
वेद अध्ययन करने से वह विप्र (ज्ञानी) बनता है,
और कर्मों (कर्तव्यों) के पालन से ब्राह्मण कहलाता है।
➡️ यानी जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, बल्कि संस्कार, शिक्षा और कर्म से बनता है।
➡️ जाति नहीं, गुण और आचरण निर्णायक हैं।
- वर्ण परिवर्तन संभव है:
“वृत्तेन वैश्वर्यगुणैः क्षत्रियो वैश्यतां व्रजेत्।
वैश्यो वा शूद्रतां याति वृत्तेनैव तु शूद्रता।।”
(मनुस्मृति 10.65)
अर्थ:
क्षत्रिय यदि अपने कर्तव्यों को छोड़कर वैश्य गुणों को धारण कर ले तो वह वैश्य बन जाता है,
वैश्य यदि शूद्र जैसे आचरण करने लगे तो वह शूद्र बन जाता है।
(इसी तरह से अन्य वर्णों में भी परिवर्तन हो सकता है।)
➡️ वर्ण स्थायी नहीं है, व्यवहार और वृत्ति (कर्म और प्रवृत्ति) के आधार पर बदल सकता है।
- सभी वर्णों में समानता का संकेत:
“सर्वं ब्रह्मेति व्यपाश्रयः।”
(मनुस्मृति 12.118)
अर्थ:
सब कुछ ब्रह्म है (अर्थात सभी में एक ही दिव्यता है)।
➡️ सभी प्राणी ब्रह्म के अंश हैं — कोई छोटा-बड़ा नहीं।
- कर्मफल पर जोर (जन्म नहीं):
“कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणा जायते कुलम्।
कर्मणा लभते स्वर्गं कर्मणा लभते यशः।।”
(मनुस्मृति 12.3)
अर्थ:
प्राणी कर्मों से जन्म लेता है, कर्मों से कुल (समाज में प्रतिष्ठा) बनती है,
कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है, कर्मों से यश प्राप्त होता है।
➡️ यहाँ भी कर्म को ही जीवन की सफलता का आधार माना है, जन्म को नहीं।
संक्षेप में:
- मनुस्मृति में जाति जन्म आधारित नहीं थी — बल्कि संस्कार, शिक्षा, कर्म पर आधारित थी।
- कालांतर में इस सिद्धांत का गलत और स्वार्थी उपयोग कर समाज को जन्माधारित वर्ण व्यवस्था में ढाल दिया गया।
- मनुस्मृति का मूल दर्शन कहीं न कहीं जातिविहीन या कर्म आधारित समाज का समर्थन करता है, भले ही बाद में उसमें अनेक विकृतियाँ जोड़ दी गईं हों।
वास्तिविकता सिर्फ ये है की पुस्तकों को हम जिस भाव से पढ़ते है उनका अर्थ हमें समझ में आता है, जैसे कुरान को आतंकवादी भी पढ़ते है और सोचते है वो सही समझे है और सही कर रहे है, और उसी कुरान को अब्दुल कलाम ने पढ़ा और वो भारत देश सशक्त बनाने में लगे रहे, ऐसे ही रिश्वत लेने वाला सरकारी कर्मचारी और ईमानदारी से काम करने वाला सरकारी कर्मचारी एक ही किताब पढ़ कर सिस्टम में आया है, तो दोष देना है तो नियत को दीजियेगा ग्रंथो को नहीं