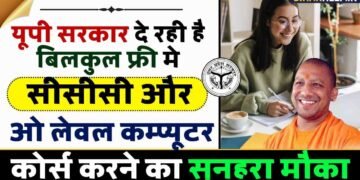भारत, एक ऐसा देश जहां “न्याय” को संविधान का आधार माना जाता है, आज अपनी ही न्याय व्यवस्था के बोझ तले दबा हुआ है। 6 करोड़ से अधिक मुकदमे देश के विभिन्न कोर्ट्स में लंबित हैं, जो न केवल न्यायिक प्रक्रिया को धीमा कर रहे हैं, बल्कि करोडो परिवारों के जीवन को भी उथल-पुथल में डाल रहे हैं। अगर हम मानें कि एक परिवार में औसतन 4 लोग हैं और प्रत्येक मुकदमे में कम से कम दो परिवार शामिल हैं, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 50 करोड़ लोग इन लंबित मुकदमों के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। यह आंकड़ा केवल एक अनुमान है; वास्तविक प्रभावित लोगों की संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। इस ब्लॉग में, हम इस संकट के प्रभाव, कारणों और जिम्मेदार पक्षों का विश्लेषण करेंगे।
लंबित मुकदमों की स्थिति: एक भयावह आंकड़ा
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार, 2025 तक भारत में कुल लगभग 5.2 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, लेकिन कुछ स्रोतों ने इसे 6 करोड़ तक होने का अनुमान लगाया है। इनमें से:
- जिला और अधीनस्थ कोर्ट्स: 4.4 करोड़ से अधिक मुकदमे (85% से अधिक)।
- हाई कोर्ट्स: लगभग 59-62 लाख मुकदमे।
- सुप्रीम कोर्ट: 82,445 मुकदमे (जनवरी 2025 तक)।
इनमें से 1.8 लाख से अधिक मुकदमे 30 साल से अधिक पुराने हैं, जिनमें कुछ 1952 से लंबित हैं। यह स्थिति न केवल न्याय व्यवस्था की नाकामी को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे लाखों लोग वर्षों तक न्याय के इंतजार में अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खो देते हैं।
50 करोड़ लोगों पर प्रभाव: एक सामाजिक त्रासदी
जब एक मुकदमा कोर्ट में लंबित रहता है, तो यह केवल वादी और प्रतिवादी तक सीमित नहीं रहता। इसके प्रभाव पूरे परिवार, समुदाय और समाज पर पड़ते हैं। आइए इसे समझते हैं:
- पारिवारिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य:
- प्रत्येक मुकदमे में कम से कम दो पक्ष शामिल होते हैं, और यदि एक परिवार में औसतन 4 लोग हैं, तो 6 करोड़ मुकदमों का मतलब है 48 करोड़ से अधिक प्रभावित लोग। यह संख्या और भी अधिक हो सकती है, क्योंकि कई मामलों में विस्तृत परिवार (रिश्तेदार, बच्चे, बुजुर्ग) भी प्रभावित होते हैं।
- लंबित मुकदमों के कारण परिवारों में तनाव, चिंता और अवसाद बढ़ता है। उदाहरण के लिए, एक संपत्ति विवाद पूरे परिवार को बांट सकता है, और आपराधिक मामले में गवाहों को बार-बार कोर्ट में उपस्थित होने की वजह से मानसिक और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है।
- कुछ मामलों में, लोग इस तनाव के कारण आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं, जैसा कि @AshwiniUpadhyay ने 2019 में एक पोस्ट में उल्लेख किया था कि 3.5 करोड़ लंबित मुकदमों के कारण 21 करोड़ लोग तनाव में थे।
- आर्थिक नुकसान:
- कोर्ट केस में शामिल होने के लिए लोग अपनी नौकरी, व्यवसाय और रोजमर्रा की कमाई को छोड़कर कोर्ट की तारीखों पर समय बिताते हैं। बार-बार सुनवाई टलने से यह आर्थिक बोझ और बढ़ जाता है।
- वकीलों की फीस, कोर्ट की प्रक्रिया और यात्रा खर्च लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति को कमजोर करते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां लोग पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, यह स्थिति उन्हें गरीबी रेखा की ओर धकेल सकती है।
- विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पिछले एक दशक में 17.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, लेकिन लंबित मुकदमों के कारण होने वाला आर्थिक बोझ इस प्रगति को प्रभावित कर सकता है।
- सामाजिक और पारिवारिक विघटन:
- संपत्ति विवाद, तलाक, और आपराधिक मामले परिवारों में दरार पैदा करते हैं। बच्चे, जो इन मुकदमों के प्रत्यक्ष प्रभाव में नहीं भी होते, माता-पिता के तनाव और आर्थिक दबाव के कारण शिक्षा और मानसिक विकास में पिछड़ सकते हैं।
- सामुदायिक स्तर पर, लंबित मुकदमे सामाजिक तनाव को बढ़ाते हैं, खासकर जब मामले सांप्रदायिक या जातिगत विवादों से जुड़े हों।
लाचार न्याय व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन?
लंबित मुकदमों की इस भयावह स्थिति के लिए कई पक्ष जिम्मेदार हैं। आइए प्रमुख कारणों और जिम्मेदार पक्षों पर नजर डालें:
- जजों और कोर्ट स्टाफ की कमी:
- इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 15 जज हैं, जो विश्व मानकों से बहुत कम है। हाई कोर्ट्स में 33% और जिला कोर्ट्स में 21% जजों के पद खाली हैं।
- अपर्याप्त कोर्ट स्टाफ और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण केसों की सुनवाई में देरी होती है।
- सरकार: सबसे बड़ा वादी:
- NJDG के अनुसार, 50% लंबित मुकदमों में सरकार स्वयं एक पक्ष है।
- सरकारी विभागों द्वारा अनावश्यक अपील दायर करना, खराब कानूनी रणनीति, और देरी से दस्तावेज जमा करना इस संकट को बढ़ाता है।
- वकीलों और पक्षकारों की रणनीति:
- कुछ वकील और पक्षकार जानबूझकर सुनवाई को टालने की रणनीति अपनाते हैं, जैसे अनुपस्थिति, गवाहों का न आना, या बार-बार स्थगन मांगना। आपराधिक मामलों में 60% देरी का कारण गवाहों या आरोपियों की अनुपस्थिति है।
- कानूनी प्रक्रिया की जटिलता:
- भारत की कानूनी प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और समय लेने वाली है। उदाहरण के लिए, साक्ष्य जुटाने, गवाहों की पेशी, और अपील प्रक्रिया में वर्षों लग जाते हैं।
- न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 जैसे कानून बोझिल हैं और न्यायिक उत्तरदायित्व को प्रभावी ढंग से लागू करने में असमर्थ हैं।
- सामाजिक और सांस्कृतिक कारक:
- भारत में मुकदमेबाजी की संस्कृति बढ़ रही है, जहां छोटे-छोटे विवाद भी कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) जैसे मध्यस्थता और सुलह का उपयोग कम होता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता की कमी के कारण लोग कोर्ट में लंबी प्रक्रिया में फंस जाते हैं।
समाधान के उपाय
इस संकट से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं:
- जजों और स्टाफ की भर्ती:
- खाली पदों को तुरंत भरा जाए और प्रति 10 लाख लोगों पर कम से कम 50 जजों का लक्ष्य रखा जाए।
- डिजिटल कोर्ट और ई-फाइलिंग:
- ई-कोर्ट परियोजना को और तेज किया जाए। ऑनलाइन सुनवाई और डिजिटल दस्तावेज जमा करने से समय की बचत होगी।
- वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR):
- मध्यस्थता, सुलह और लोक अदालतों को बढ़ावा देना चाहिए। 2023 में लोक अदालतों ने लाखों मामलों का निपटारा किया, जो एक सकारात्मक उदाहरण है।
- सरकारी मुकदमों में सुधार:
- सरकार को अनावश्यक अपील दायर करने से बचना चाहिए और केस प्रबंधन को बेहतर करना चाहिए।
- कानूनी जागरूकता:
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को कानूनी प्रक्रिया और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना जरूरी है।
भारत की न्याय व्यवस्था में 6 करोड़ लंबित मुकदमे केवल आंकड़े नहीं हैं; ये लाखों परिवारों की उम्मीदों, सपनों और जीवन का सवाल हैं। 50 करोड़ से अधिक लोग इस संकट के कारण आर्थिक, मानसिक और सामाजिक उथल-पुथल का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति न केवल न्यायिक प्रणाली की कमियों को उजागर करती है, बल्कि समाज के हर स्तर पर सुधार की मांग करती है। सरकार, न्यायपालिका, वकील, और समाज सभी को मिलकर इस लाचार व्यवस्था को सुधारने की दिशा में काम करना होगा।
क्या भारत में कोर्ट कम है ?
क्या भारत में कोर्ट कम है ? इस प्र्शन का उत्तर में कुछ आंकड़े देता हूँ आप खुद सोचियेगा, भारत में सुप्रीम कोर्ट एक है जिसमे 34 (मुख्य न्यायाधीश + 33 अन्य जज) जज होते है, हाई कोर्ट 25 है, इसमें भी प्रत्येक कोर्ट में अनुमानित जजों की संख्या 90 से 160 के बीच होनी चाहिए, अब बात जिला स्तर पर तो यहाँ भी प्रति जिले में कम से कम 20 से 30 जज होते है यानि सभी जिलों का मिलकर 5000 से ऊपर जज मिलेंगे, अब आप सोचिये की क्या देश के सभी कोर्ट के जज जो की एक आरामदायक जीवन जीने के चाहत रखते है इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए पर्याप्त है या नहीं
आप क्या सोचते हैं? क्या यह संकट हल हो सकता है, या यह भारत की नियति बन चुकी है? अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस ब्लॉग को शेयर करें ताकि अधिक लोग इस गंभीर मुद्दे के बारे में जागरूक हों।
स्रोत:
- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG): njdg.ecourts.gov.in
- इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025
- विश्व बैंक रिपोर्ट 2025
- X पोस्ट