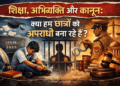अब भारत में किसी छात्र की आत्महत्या केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रह गयी अगर वो किसी गैर सवर्ण यानि गैर सामान्य वर्ग के स्टूडेंट ने की हो तो वह बहुत जल्दी सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक बहस में बदल जाती है। लेकिन यह बहस हर मामले में समान रूप से नहीं होती यानि अगर सामान्य वर्ग का या सवर्ण स्टूड्न्ट आत्महत्या करता है तो । यही सामाजिक असमानता आज सबसे बड़ा प्रश्न बन चुकी है।
जब एक दलित या आदिवासी छात्र की आत्महत्या होती है, तो मामला अक्सर राष्ट्रीय समाचार बनता है। मीडिया स्टूडियो गरम हो जाते हैं, बयानबाज़ी शुरू हो जाती है, संस्थानों पर आरोप लगते हैं, और कई बार बिना किसी न्यायिक निष्कर्ष के ही सवर्ण समाज को सामूहिक दोषारोपण कर दिया जाता है।
कहा जाता है कि “संस्थानिक भेदभाव” है, “सवर्ण मानसिकता” है, “शिक्षक और व्यवस्था ज़िम्मेदार हैं”। इसी तर्क के सहारे यह भी कहा जाता है कि UGC नियम, आरक्षण और विशेष प्रावधान और कठोर होने चाहिए, क्योंकि कथित तौर पर सवर्ण समाज के लोग अन्य वर्गों के छात्रों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं।
अब ज़रा दूसरा दृश्य देखिए।
IIT बॉम्बे में छात्र की आत्महत्या: एक खामोश खबर
IIT बॉम्बे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में एक बी.टेक. छात्र, राजस्थान निवासी नमन अग्रवाल, हॉस्टल की छत से कूदकर आत्महत्या कर लेता है।
यह घटना दुखद है, हिला देने वाली है — लेकिन क्या यह उसी तीव्रता से राष्ट्रीय बहस बनती है?
आमतौर पर नहीं।
कुछ खबरें आती हैं, कुछ पंक्तियाँ लिखी जाती हैं, “व्यक्तिगत कारण”, “मानसिक तनाव”, “पढ़ाई का दबाव” जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं, और मामला धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है।
न कोई वर्ग दोषी ठहराया जाता है, न कोई सामाजिक समूह कटघरे में खड़ा होता है, न ही यह कहा जाता है कि “पूरी व्यवस्था ज़िम्मेदार है”।
सवाल छात्र का नहीं, नज़रिए का है
यह लेख यह नहीं कहता कि किसी भी छात्र की आत्महत्या कम या ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
हर मृत्यु समान रूप से दुखद है क्युकी ये उसके परिवार के पूर्ण क्षति है ।
लेकिन सवाल यह है कि:
- क्या देश में हर आत्महत्या को देखने का पैमाना समान है?
- क्या किसी की मौत पर शोक और किसी की मौत पर राजनीति करना न्यायसंगत है?
- क्या जाति के आधार पर संवेदनशीलता तय होनी चाहिए?
यदि आत्महत्या का कारण वास्तव में संस्थानिक दबाव, मानसिक स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और अकेलापन है, तो वह समस्या हर छात्र के लिए है — उसकी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, आखिर संविधान भी तो यही कहता है की राज्य जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन सामान्य वर्ग के स्टूडेंट के साथ तो इसीलिए किया जाता है क्युकी वो समान्य वर्ग में आते है ।
मौत पर भी राजनीति?
सबसे पीड़ादायक बात यह है कि कई बार मृत्यु के बाद भी राजनीतिक रोटियाँ सेंकी जाती हैं।
मृतक का जीवन, उसकी मानसिक स्थिति, उसके संघर्ष — सब पीछे छूट जाते हैं, और आगे आ जाता है एक ऐसा नैरेटिव, जो पहले से तय होता है।
यह न तो उस छात्र के साथ न्याय है,
न ही उस समाज के साथ,
और न ही उस लोकतंत्र के साथ, जो समानता का दावा करता है।
लोकतंत्र और संविधान पर असहज प्रश्न
भारत का संविधान समानता, न्याय और गरिमा की बात करता है।
लोकतंत्र का अर्थ है — हर नागरिक का दुख समान रूप से सुना जाना।
तो फिर यह सवाल उठना स्वाभाविक है:
क्या हम वास्तव में एक ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जहाँ हर नागरिक की पीड़ा समान मानी जाती है?
या फिर कुछ पीड़ाएँ ज़्यादा “उपयोगी” मानी जाती हैं?
यह प्रश्न किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं है।
यह प्रश्न चयनित संवेदनशीलता, चयनित आक्रोश और चयनित न्याय के खिलाफ है।
निष्कर्ष: सोचने की ज़रूरत है
छात्र आत्महत्याएँ:
- जाति की लड़ाई नहीं हैं,
- वैचारिक हथियार नहीं हैं,
- और न ही राजनीतिक औज़ार होनी चाहिए।
ये एक संकेत हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक अपेक्षाएँ और मानसिक स्वास्थ्य ढाँचा गंभीर संकट में है।
जब तक हम हर छात्र को — बिना लेबल लगाए — सिर्फ एक इंसान की तरह नहीं देखेंगे,
तब तक न न्याय पूरा होगा,
न लोकतंत्र,
और न ही संविधान की आत्मा।
अब भी समय है — सोचने का, ठहरने का, और ईमानदारी से सवाल पूछने का।