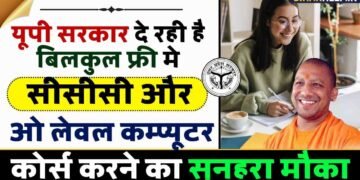राधिका की हत्या: दोष किसका?
👉 पिता दोषी है?
हां — क्योंकि
- उसने अपनी संतान की जान ली, जो कि किसी भी धर्म, संविधान या मर्यादा से परे है।
- उसने “इज्ज़त” के नाम पर हत्या की — लेकिन इज्ज़त हत्या से कभी नहीं बचती, वो तो और धूल में मिल जाती है।
- वह अपनी भावनाओं, अपने डर और क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सका — यह उसकी हार थी।
👉 बेटी दोषी है?
नहीं — परंतु
- क्या उसने उस परवरिश, उस मानसिकता, उस समाज की संवेदनशीलता को समझा?
- क्या उसने अपने आत्म-अभिव्यक्ति और सामाजिक पहचान की यात्रा में यह सोचा कि उसका घर, उसके माता-पिता उससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं?
नारी का स्वतंत्र होना गलत नहीं, परंतु उस स्वतंत्रता को “दिखावे और आघात” का रूप देना समाज में टकराव को जन्म देता है।
👉 या दोषी हैं हम सब…?
- क्योंकि हमने संस्कृति के नाम पर रूढ़ियाँ, और आधुनिकता के नाम पर विद्रोह परोसा है।
- क्योंकि हम ये तो कहते हैं कि “बेटियाँ हमारी शान हैं”, लेकिन जब वही बेटियाँ अपने तरीके से जीने लगती हैं, तो हमारी “शान को धक्का” लगता है।
- क्योंकि हमने बच्चों को सपने देखना सिखाया, लेकिन समाज और परिवार को उन सपनों की भाषा नहीं सिखाई।
हम बहना तो चाहते हैं… लेकिन बहते हुए दिशा खो बैठे हैं…
“हम बहना तो चाहते हैं, और बह भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं जा कहाँ रहे हैं… हमारा अंत क्या होगा?”
— यही इस पूरे युग की सबसे बड़ी त्रासदी है।
हम आज संस्कृति और आधुनिकता के बीच झूल रहे हैं,
हमारी जड़ें मिट्टी में थीं, लेकिन अब सिर खुले आसमान में है, और पाँव ज़मीन से कट चुके हैं।
क्या हल है?
- संवेदना से भरा संवाद:
- पिताओं को बेटियों की सोच को सुनना सीखना होगा।
- बेटियों को भी परिवार के मूल्यों को समझते हुए अपने कदम रखने होंगे।
- संस्कृति और आधुनिकता का समन्वय:
- नारी अगर टेनिस अकादमी चलाना चाहती है, तो करे — पर घरवालों से भागकर नहीं, उन्हें साथ लेकर।
- और समाज को यह समझना होगा कि इंस्टाग्राम पर रील बनाना अपराध नहीं है, अपराध तब होता है जब आप अपनी बेटी को उसकी पहचान से वंचित कर देते हैं।
- घुटन से मुक्ति और उन्मुक्ति से संयम:
- न लड़की को घुटन में जीने दें, न उसे ऐसी उन्मुक्तता दें जो समाज को चौंका दे।
- मध्य मार्ग ही शिव का मार्ग है।
एक सवाल छोड़ता हूँ:
“अगर हम अपने बच्चों को उड़ने का हक़ देंगे,
तो क्या हमें उनकी ऊंचाई से डरना चाहिए —
या गर्व करना चाहिए?”
कभी एक समय था, जब घर की स्त्रियाँ परिवार की आत्मा मानी जाती थीं। वे वही स्त्रियाँ थीं, जिन्होंने न केवल चूल्हे-चौके में स्वाद भरा, बल्कि हर रिश्ते में रस भी डाला। वे सास-बहू, ननद-भाभी, मां-बेटी सभी रिश्तों को इस सूझ-बूझ से निभाती थीं कि समाज में सामंजस्य और सहजीवन की परंपरा चलती रही।
लेकिन तभी इतिहास ने मोड़ लिया। पश्चिमी विचारधारा, जिसे हमने बिना आत्ममंथन के आधुनिकता का नाम दे दिया, हमारे दरवाज़े से घुसकर हमारे परिवार की जड़ें ही खोदने लगी।
एक वर्ग ने रचा विचारों का षड्यंत्र
एक ऐसा वर्ग खड़ा हुआ जिसने स्त्रियों की वास्तविक क्षमता को पहचानने के बजाय, उन्हें एक ऐसे रास्ते पर मोड़ा जहाँ से घर-परिवार गौण हो गया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही जीवन का अंतिम सत्य बता दिया गया।
“स्त्री को रसोई से बाहर निकालो, कमाई के मैदान में लाओ, तभी वह स्वतंत्र होगी” — इस विचार को इस तरह प्रचारित किया गया जैसे कि घर संभालना किसी ग़ुलामी से कम हो।
जो स्त्रियाँ परिवार को संभालने का कौशल रखती थीं, उन्हें कहा गया कि “तुम पिछड़ी हो, तुम आत्मनिर्भर नहीं हो, तुम पुरानी सोच वाली हो”।
उन्हें मानसिक रूप से इस कदर नीचा दिखाया गया कि उनके भीतर का आत्मगौरव भी स्वयं की भूमिका पर लज्जा करने लगा।
कामकाजी महिला या ‘घर से दूर’ मानसिकता?
अब स्त्रियाँ घर से बाहर निकलीं — यह कोई आपत्ति की बात नहीं। पर जिस मानसिकता से वे निकलीं, वह सोचने लायक है। उन्हें बताया गया कि:
- “तुम्हारा असली मूल्य घर से बाहर कमाने में है।”
- “तुम जितना कमाओगी, उतनी ही स्वतंत्र होगी।”
- “घर को जोड़ना तुम्हारा दायित्व नहीं, गुलामी है।”
अब परिणाम देखिए —
स्त्रियाँ दैनिक वेतन में तो आत्मनिर्भर हो गईं, पर उनकी मानसिकता अब घर को एक बोझ समझने लगी।
वही माँ, वही पति, वही बच्चे — जिनके लिए पहले वह जूझती थीं — अब उनकी प्राथमिकता में दूसरे पायदान पर आ गए।
कपड़ों में ‘विकास’ का पैमाना?
“कम से कम कपड़े और ज़्यादा से ज़्यादा दिखावा” — यही आधुनिक सोच की पहली परिभाषा बना दी गई।
और यह प्रचार भी इस तरह हुआ कि
- जो लड़की शालीन वस्त्र पहनती है, वह ‘संकीर्ण सोच’ की कहलाए
- और जो लड़की अपने शरीर का प्रदर्शन करती है, वह ‘बोल्ड और कॉन्फिडेंट’ कहलाए
क्या स्त्री की आत्मनिर्भरता उसके वस्त्रों की लंबाई से तय की जाएगी?
यह एक चालाक, सुनियोजित सांस्कृतिक युद्ध था, जिसमें स्त्री को उसके ही अस्त्र से हराया गया — उसकी गौरवमयी पारिवारिक भूमिका को ध्वस्त कर दिया गया।
कुछ सच्ची कहानियाँ…
- रीना — जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, पर जब उसकी माँ बीमार हुई, और उसने छुट्टी माँगी तो बॉस ने कहा — “You are a professional, not a caregiver.”
तब उसने सोचा — “क्या सच में काम से ज़रूरी माँ नहीं?” - एक प्रोफेसर, जो महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान देती हैं, उन्होंने खुद बताया —
“जब मेरी बेटी ने कहा कि वो सिर्फ गृहिणी बनना चाहती है, तो मुझे शर्म महसूस हुई। फिर मैंने सोचा — मैंने क्या सीखा और सिखाया?”
पुरुष = अत्याचारी? लेख = पितृसत्ता?
और जो सबसे विडंबना की बात है —
जब भी कोई ऐसा लेख लिखा जाता है जो घर-परिवार, स्त्री की पारंपरिक भूमिका, संस्कृति और संतुलन की बात करता है, तो लेखक पर ठप्पा लग जाता है —
“यह पितृसत्ता को बढ़ावा दे रहा है”
और हाँ, ऐसा ताना मारने वाले भी पुरुष ही होता है… पिता ही होता है… भाई ही होता है…
क्योंकि समाज में यह भी एक ट्रेंड बन गया है कि
- पुरुष अगर स्त्री के सम्मान की बात करे, तो वह ‘दमनकारी’ कहलाता है।
- और यदि स्त्री स्वयं अपने पारिवारिक गौरव की बात करे, तो वह ‘पीड़ित मानसिकता’ की प्रतीक बना दी जाती है।
निष्कर्ष: स्वच्छंदता नहीं, संतुलन चाहिए
हम ये नहीं कह रहे कि स्त्री को बाहर काम नहीं करना चाहिए।
हम ये कह रहे हैं कि स्त्री की शक्ति उसकी संतुलनकारी बुद्धि में है, न कि सिर्फ तनख्वाह या टाइट पहनने की स्वतंत्रता में।
स्वतंत्रता का मतलब कभी भी परिवार को पीछे छोड़ना नहीं था।
वह तो था — घर, समाज और स्वयं के बीच समरसता बनाना।
अब ज़रूरत है…
- सोचने की — क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं?
- और उठने की — एक ऐसी सोच के लिए, जो स्त्री को उज्ज्वल, स्वस्थ, सम्मानित और सशक्त बनाए — लेकिन अपनों से काट कर नहीं, अपनों के साथ जोड़ कर।
“हर वो विचार जो घर तोड़ दे, वो स्वतंत्रता नहीं षड्यंत्र है।”
✍️ – एक ‘पितृसत्तात्मक’ सोच रखने वाला बेटा, भाई और पति… जो स्त्री को देवी भी मानता है और शक्ति भी।